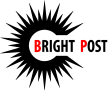साहित्य बनाम प्रसिद्धि
– पाठक बेशुमार परन्तु अस्तित्व रहा सिसक….
वरिष्ठ पत्रकार- सलीम रज़ा
देहरादून। साहित्य समाज का दर्पण है, लिहाजा लेखक का ये कर्म है कि, वो समाज के इर्द-गिर्द घटित हो रही घटनाओं, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादी परम्पराओं और समाज को दूषित कर रहे घटक तत्वों को अपनी लेखनी से कलमवद्ध कर समाज में सकारात्मक उर्जा लाने के लिए अपना योगदान करे। लेंकिन बेहद दुःख का विषय है कि, समकालीन समय के दौर में साहित्य लेखन अपनी सकारत्मकता वाली पहचान खोता जा रहा है। आज के दौर का लेखक लगता है कि, चकाचौंध भरी दुनिया में रूपहले परदे से प्रेरित होकर भड़कीले विज्ञापनों की तरह प्रसिद्धि पाकर रातों-रात अपनी मार्केटिंग बढाने की शुगल में लग गया, और साहित्य के सकारत्मक रूख को अलविदा करके नकारात्मक जैसे दूषित पथ पर ले जाने का काम कर रहा है।
अनायास ऐसा महसूस होने लगा है कि, लेखन का दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है और अपनी लक्ष्मण रेखा खींचकर सीमित सा हो गया है। अमूमन ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि, न तो साहित्य में कथानक ही ठीक होता है और न ही कथावस्तु उस पर सोने पे सुहागा, ये होता है कि लेखक इतना तन्मय होकर लिखता है कि, उसे कथा चित्रण का घ्यान ही नहीं होता, उसकी कथा में ग्रीष्म त्रतु का चित्रण होता है, लेकिन बालकनी में रखे गमलों में गुलदाउदी के फुल खिले दिखाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि, आज के लेखकों में प्रसिद्धि पाने की जैसे होड़ सी लगी हुई है। ऐसे में कथानक की छीछालेदर तो होनी ही है। फिर उसके विषय भी आम नहीं रह जाते, वो भी मार्केट में बिकने वाली सीजनल सब्जी की तरह खास हो जाते हैं।
साहित्य लेखन समय के साथ करवटें बदलने वाला नहीं है, लेकिन आज के दौर का लेखक जबरन अपनी लेखनी को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि, शायद वो इस भ्रम का कीड़ा पाल रहा हो कि, साहित्य तो बिन पतवार की नाव है। जिसको सिर्फ और सिर्फ वो ही सहारा देकर किनारे लगाने का अथक प्रयास कर रहा है। आज के दौर में विलक्षण प्रतिभा के धनी लेखकों के कथानक में पात्र बहुतायत मात्रा में ऐसे मिलेंगे जो विलासिता का जीवन यापन करने वाले होंगे। जिस पर वो अपनी लेखनी को सरपट दौड़ायेगा, लेकिन उसके कथानकों में आंचल में दुधमुंहा बच्चा और उस हांड मांस की मुरझाये स्तन वाली मां और निरीह शरीर वाला वो जिसकी सांस भारी बोझ उठाने से फूल रहीं हों, ऐसे लड़खड़ाते वृद्ध और सड़क के किनारे रखे डस्टबिन में उतरकर खाना तलाशते नौनिहाल जैसे पात्र क्यों हाशिये पर रह जाते है?
क्या समयानुसार आज के लेखकों ने भी अपनी मानसिक संवेदनाओं को अलग रखकर ऐसे पात्रों को तिलांजलि दे दी जो देश की संघीय प्रणाली का दंश झेल रहे हैं? उनकी रचनाओं में ऐसे पात्र क्यों गुम हो रहे हैं? जबकि कथा सम्राट मुशी प्रेमचंद जी ने तो जानवरों को भी पात्र बनाकर लोंगों को उनका मर्म समझा दिया था। दुःखद है कभी अन्याय और संघर्ष के खिलाफ भागने वाली कलम को आज के युग के लेखकों ने प्रसिद्धि और चाटुकारिता का लिबास पहनाकर कम समय में शोहरत दिलाने वाली स्वार्थपरक प्लेटिनम की बैसाखी पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां पाठक बेशुमार हैं। लेकिन अस्तित्व सिसक रहा है।