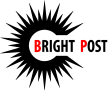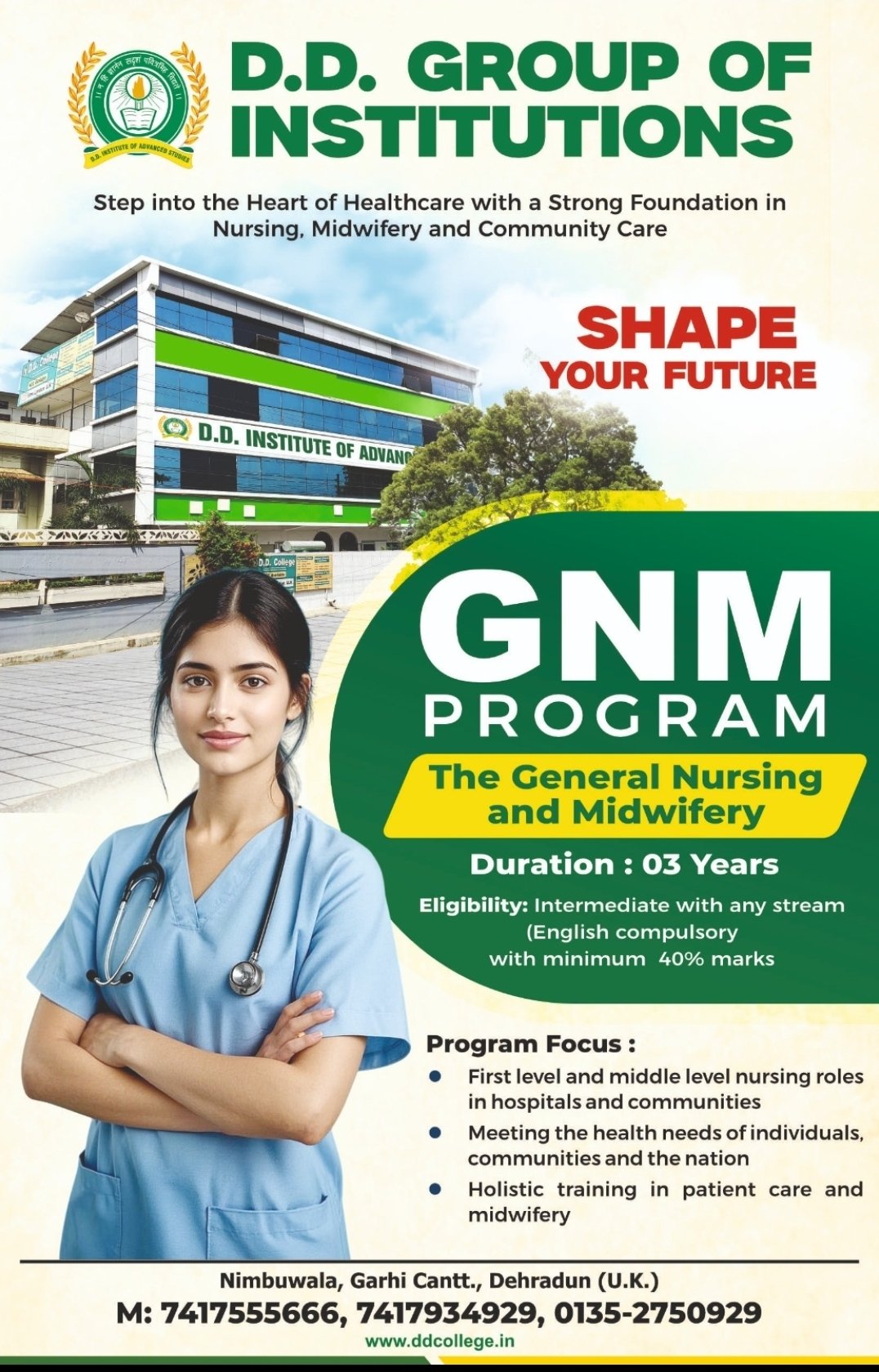उत्तराखंड में वनाधिकार कानून की हकीकत। 97% दावे खारिज, क्यों हो रहे लोग हक से वंचित?
उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान पहाड़ों, नदियों और हरे-भरे जंगलों से है। यहां का 71 प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है। जंगल केवल प्रकृति की धरोहर ही नहीं बल्कि यहां रहने वाले लाखों लोगों के जीवन, आजीविका और संस्कृति का भी हिस्सा हैं।
पीढ़ियों से लोग जंगलों पर निर्भर हैं, कभी ईंधन के लिए, कभी चारे के लिए, तो कभी रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए। लेकिन यही जंगल जब कानून और दावों के जाल में फंस जाते हैं, तो सवाल उठता है कि असल में किसका अधिकार बनता है और कौन इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है।
वनाधिकार कानून क्या है?
साल 2006 में संसद ने वनाधिकार कानून (Forest Rights Act-2006) पारित किया। इसका मकसद था आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों को जंगलों में रहने और आजीविका का कानूनी अधिकार देना।
कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसे 2008 में लागू करवाया। इस कानून के तहत व्यक्ति या समुदाय दावा कर सकता है कि वह तीन पीढ़ियों से जंगल में रह रहा है या जंगलों पर निर्भर है। सही सबूत मिलने पर उसे जमीन का अधिकार (टाइटल) मिल जाता है।
उत्तराखंड की चौंकाने वाली स्थिति
उत्तराखंड में अब तक 6,800 दावे पेश किए गए। लेकिन इनमें से केवल 186 दावों को मंजूरी मिली है। 40 दावे अभी विचाराधीन हैं, जबकि करीब 6,574 दावे खारिज कर दिए गए। यानी यहां अस्वीकृति दर 97 प्रतिशत है। यह स्थिति पूरे देश में सबसे खराब कही जा सकती है।
राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अब तक 51,23,104 दावे पेश हुए हैं। इनमें से 25,11,375 दावे स्वीकार हुए, जबकि 18,62,056 खारिज हो गए। लगभग 7.5 लाख दावे अभी भी लंबित हैं। यानी राष्ट्रीय औसत से लगभग आधे दावों को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड का आंकड़ा इसकी तुलना में बेहद निचले स्तर पर है।
पड़ोसी राज्यों की तस्वीर
- हिमाचल प्रदेश: यहां 5,566 दावे दर्ज हुए। इनमें से 808 मंजूर, केवल 54 खारिज और बाकी 4,704 दावे विचाराधीन हैं।
- उत्तर प्रदेश: यहां 94,166 दावे आए। इनमें से 23,430 मंजूर और केवल 736 खारिज हुए।
स्पष्ट है कि उत्तराखंड में दावों का खारिज होना न केवल असामान्य है बल्कि कहीं न कहीं प्रणालीगत खामियों की ओर इशारा करता है।
प्रमुख वन संरक्षक का पक्ष
उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) समीर सिन्हा का कहना है कि,“फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावों का तीन चरणों में परीक्षण होता है। यदि इतने अधिक दावे गलत साबित हो रहे हैं तो या तो लोग पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर पा रहे हैं या फिर दावे ही गलत हैं। समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर परीक्षण किया जाता है और सही पाए जाने पर ही टाइटल दिए जाते हैं।”
इस बयान से साफ है कि वन विभाग इसे गलत दावों और दस्तावेज़ों की कमी का मामला मानता है।
अस्वीकृति के कारण
उत्तराखंड में लगभग 97 प्रतिशत दावों के खारिज होने के पीछे कई वजहें सामने आती हैं:-
- दस्तावेजों की कमी – कानून के तहत तीन पीढ़ियों का रिकॉर्ड जरूरी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह उपलब्ध नहीं होता।
- राजस्व रिकॉर्ड का अभाव – कई दावेदार जिस जमीन पर दावा करते हैं, वह फॉरेस्ट रिकॉर्ड या ग्राम सभा के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं होती।
- निवास का सबूत नहीं – यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि दावेदार वाकई तीन पीढ़ियों से वहां रह रहा है।
- कानून का दुरुपयोग – कई बार ऐसे लोग भी दावा करते हैं जिनका सीधा संबंध जंगल से नहीं होता, ताकि वे जमीन का फायदा उठा सकें।
किसके दावे होते हैं?
उत्तराखंड में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावे आमतौर पर वन गुर्जरों, पारंपरिक जनजातियों और जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों द्वारा किए जाते हैं। इनका सीधा ताल्लुक जंगल से होता है और ये लोग पट्टे, लीज या जमीन पर अधिकार की मांग करते हैं।
राजनीतिक आवाज़ें
बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि, “जिन लोगों के दावे खारिज हुए हैं, उनके पास अब कोर्ट का ही सहारा बचा है। लेकिन कोर्ट में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट राइट एक्ट को नए रूप में परिभाषित किया जाए।”
वे यह भी मानते हैं कि इस मामले को समाज कल्याण विभाग को सौंपना सही नहीं था और निर्णय की प्रक्रिया वन विभाग के माध्यम से होनी चाहिए।
स्थानीय कहानियां: हक से वंचित लोग
गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांवों में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जहां लोग तीन पीढ़ियों से जंगल में रहते आए हैं लेकिन दस्तावेज़ न होने के कारण उनका दावा खारिज हो गया।
उदाहरण के लिए, चमोली जिले के एक गुर्जर परिवार का कहना है कि उनके दादा और पिता दोनों यहीं के जंगलों में रहते थे, लेकिन कोई राजस्व रिकॉर्ड न होने से उनका दावा निरस्त कर दिया गया।
इसी तरह पौड़ी के कुछ गांवों में ग्रामीण कहते हैं कि वे जंगल से लकड़ी और चारा लाते हैं, लेकिन उन्हें कानूनी हक नहीं मिला। इससे न केवल उनका आजीविका संकट में है बल्कि जंगल और ग्रामीणों के बीच टकराव भी बढ़ रहा है।
विशेषज्ञों की राय
कई समाजशास्त्री और पर्यावरणविद मानते हैं कि कानून को लागू करने में प्रशासनिक अक्षमता सबसे बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि असली वनवासी अपने हक से वंचित हो रहे हैं जबकि कागजी प्रक्रिया के चलते झूठे दावेदार भी सामने आ रहे हैं।
भविष्य की दिशा
उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, जहां जीवन और जंगल एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सही क्रियान्वयन बेहद जरूरी है। जरूरत है कि—
- दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
- असली वनवासियों को पहचानने के लिए ग्राम स्तर पर ठोस सर्वे कराया जाए।
- झूठे दावों पर सख्त कार्रवाई हो।
- राजनीति से ऊपर उठकर वनवासियों को उनका अधिकार दिलाने की कोशिश की जाए।
उत्तराखंड में फॉरेस्ट राइट एक्ट की असली तस्वीर बेहद उलझी हुई है। एक ओर असली हकदार दस्तावेज़ों की कमी के कारण न्याय से वंचित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर झूठे दावों की भरमार कानून को कमजोर कर रही है।
सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार और केंद्र मिलकर इस कानून को व्यवहारिक रूप देंगे, या फिर आने वाले वर्षों में भी यह मुद्दा कागजी लड़ाई और कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसा रहेगा।