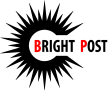उत्तराखंड का मानसून। कुदरत की मार या हमारी नीतियों की विफलता ?
- 45 दिनों में 25 लोगों की मौत, 08 लापता, 2,290 सड़कें क्षतिग्रस्त
उत्तराखंड में बारिश अब सिर्फ मौसमी घटना नहीं, एक नियमित आपदा बन चुकी है। हर साल मॉनसून के आगमन के साथ राज्य पर आफत टूट पड़ती है। इस साल भी वही हुआ—अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है, 8 लोग लापता हैं और हजारों लोग प्रभावित हैं।
2,290 सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पहाड़ों में भूस्खलन आम हो चुका है और दर्जनों राजमार्ग आज भी बंद पड़े हैं। सवाल है—क्या यह सिर्फ ‘प्राकृतिक आपदा’ है, या हमारी विकास की अंधी दौड़ का नतीजा?
बारिश, भूस्खलन और सड़कें टूटने की घटनाएं अब खबर नहीं रहीं, बल्कि “रूटीन” बन गई हैं। उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक संरचना को बिना सोचे-समझे छेड़ा गया है।
अवैज्ञानिक निर्माण, अवैध खनन और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रति और भी संवेदनशील बना दिया है। और फिर हम इस त्रासदी को “कुदरत का कहर” कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं।
प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव का यह कहना कि “स्थिति सामान्य है“, न केवल संवेदनहीनता दिखाता है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठाता है। अगर यह “सामान्य” है, तो फिर “असामान्य” क्या होगा?
राज्य सरकार दावा कर रही है कि जिलाधिकारियों को अधिक अधिकार और ₹300 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। SDRF के तहत केंद्र सरकार से ₹455.60 करोड़ की सहायता भी मिली है। लेकिन पिछले साल ₹515 करोड़ खर्च होने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या ये आंकड़े भी हमारी विफलता की कहानी नहीं कहते?
हर साल यही दृश्य दोहराया जाता है—पहले चेतावनी, फिर तबाही, फिर राहत-बचाव और अंत में भूल जाना। यह चक्र टूटेगा तब, जब आपदा प्रबंधन केवल “रिएक्टिव” नहीं, “प्रोएक्टिव” यानी पूर्व-सक्रिय होगा। जब निर्माण नीति में पारिस्थितिकी को महत्व मिलेगा। जब गांव-गांव तक लोक चेतना फैलाई जाएगी और स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन में हिस्सेदार बनाया जाएगा।
उत्तराखंड की त्रासदी सिर्फ एक राज्य की नहीं, समूचे हिमालयी क्षेत्र के लिए चेतावनी है। अगर हमने समय रहते नहीं सोचा, तो अगली आपदा कहीं ज़्यादा भयावह होगी—और तब कोई आंकड़ा, कोई बजट और कोई “सचिव का बयान” लोगों की जान नहीं बचा पाएगा।
उत्तराखंड को चाहिए एक नया विकास मॉडल—जो टिकाऊ हो, पारिस्थितिकी पर आधारित हो और स्थानीय जनहित को केंद्र में रखे। वरना, हर साल जुलाई-अगस्त में हम यही संपादकीय फिर से लिखने को मजबूर होंगे।